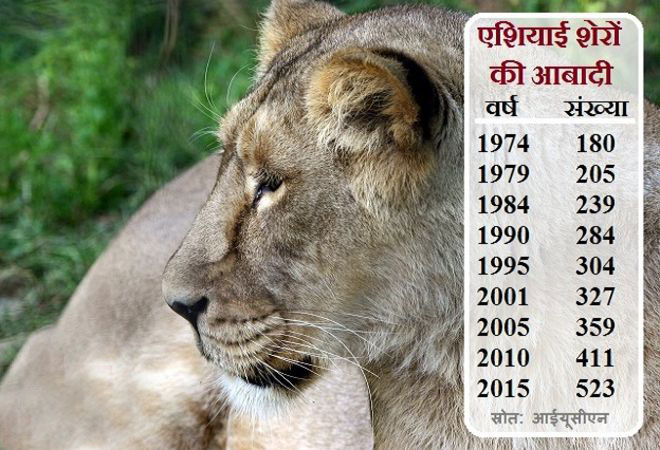
17-Sep-2016 07:00 AM
1235107
वन क्षेत्र वन्य प्राणियों और आदिवासियों के निवास क्षेत्र हैं। आदिवासियों को जंगलों का मालिक माना जाता है। लेकिन विसंगति यह है कि देश में लगभग 1150 खरब रुपए का वन क्षेत्र और संपदा होने के बाद भी आदिवासी आज भी गरीब हैं। इसको लेकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 में चिंता जताई गई है। दरअसल, यह चिंता का विषय भी है। क्योंकि जंगलों के बढ़ते औद्योगिक उपयोग ने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का विस्थापन बढ़ा दिया है। आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं और संस्कृति के खत्म होने की चिंता कर रहा है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार, वर्तमान में भारत का वन 701,673 वर्ग किलोमीटर यानी 21.34 फीसदी क्षेत्र तक फैला है जबकि 29 वर्ष पहले यह 640,819 वर्ग किलोमीटर तक फैला था। यह वृद्धि का स्पष्टीकरण पेड़ों को लगाने, विशेष रूप से मोनोकल्चर के जरिए बताया गया है, जो परिवर्तित प्राकृतिक वनों का स्थान नहीं लेते हैं एवं और स्थायी रूप से खत्म हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 30 वर्षों में वनों के स्थान पर 23,716 औद्योगिक परियोजनाएं शुरू हुई हैं। यानी औद्योगिकरण, शहरीकरण और जंगलों में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के कारण देशभर के वनों में अतिक्रमण हो रहा है। इस कारण पिछले तीन दशकों में भारत के वन का 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र साफ कर दिया गया है। सबसे बड़ा क्षेत्र (4947 वर्ग किलोमीटर) खनन को दिया गया है। रक्षा परियोजनाओं को 1,549 वर्ग किलोमीटर और जल विद्युत परियोजनाओं के 1,351 वर्ग किमी क्षेत्र दिया गया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 30 वर्षों में हरियाणा के करीब दो-तिहाई आकार के वन अतिक्रमण (15,000 वर्ग किलोमीटर) और औद्योगिक परियाजनाओं (14,000 वर्ग किमी) की भेंट चढ़ गए हैं और जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि कृत्रिम वन इनकी जगह नहीं ले सकते हैं।
भारत के जंगल समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से भी। देश के जंगलों की कीमत लगभग 1150 खरब रुपये आंकी गई है। ये भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तो कम है लेकिन कनाडा, मेक्सिको और रूस जैसे देशों के सकल उत्पाद से ज्यादा है। इसके बावजूद यहां रहने वाले आदिवासियों के जीवन में आर्थिक दुश्वारियां मुंह बनाये खड़ी रहती हैं। आदिवासियों की विडंबना यह है कि जंगलों के औद्योगिक इस्तेमाल से सरकार का खजाना तो भरता है लेकिन इस आमदनी के इस्तेमाल में स्थानीय आदिवासी समुदायों की भागीदारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। हाल ही में संसद से पारित हुए प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि विधेयक यानी कैम्पा बिल पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का मानना है कि यह विधेयक आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस विधेयक में वन अधिकार कानून, 2006 के प्रावधान को लागू करने के प्रावधान नहीं हैं।
यह विधेयक राज्यों को धन पाने का जरिया उपलब्ध कराता है, लेकिन वे इस पैसे का उपयोग आदिवासियों के विकास के लिए नहीं बल्कि उनका दमन करने के लिए करेंगे। भारत के पास कुल 701,673 वर्ग किलोमीटर जंगल है। विभिन्न प्रकार के जंगलों की कीमत 10 लाख से लेकर 55 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। भारत सरकार ने 1980 के बाद से करीब 13 लाख हेक्टेयर जंगल को गैर जंगल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। औद्योगिक समूह वन भूमि के इस्तेमाल के बदले मुआवजे के तौर पर कंपनेसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में पैसा जमा करते हैं। इसके लिए कैम्पा बनाया गया है। कानून के तहत सरकार कैम्पा को संवैधानिक दर्जा देगी जो फंड के इस्तेमाल का काम देखेगी। फंड का 90 प्रतिशत राज्यों के पास और 10 प्रतिशत केंद्र के पास रहेगा। ऐसे में सरकारों को तो लाभ मिलेगा लेकिन जंगल में रहने वाले आदिवासियों को क्या फायदा होगा। यानी उनकी गरीबी, बदहाली कम होने की बजाए और बढ़ती जाएगी।
सरकार की दोहरी नीति घातक
देश की भांति मध्यप्रदेश में भी जंगल और जंगल के अधिकार का सवाल उलझा दिया गया है। यहां उलझा दिया गया कहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमेशा से जंगलों पर राज्य या सरकारी सत्ता का नियंत्रण नहीं रहा है। वास्तव में अकूत प्राकृतिक संसाधनों का नियमन करने में कोई बुराई नहीं है किन्तु जंगलों के सम्बन्ध में जो कानून बने उनका मकसद समाज के एक खास तबके को लाभ पहुंचाना रहा है और इसी भेदभावपूर्ण नजरिए के कारण आंतरिक संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। मध्य प्रदेश सरकार की भी ऐसी ही दोहरी नीति के कारण प्रदेश के जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जंगल बचाने और बढ़ाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं वहीं दूसरी तरफ इन्हीं जंगलों में खदानों को अनुमति देकर राजस्व कमा रही हैं। सरकार की इस दोहरी नीति के कारण जंगल में माफिया हावी हो गए है।
-श्याम सिंह सिकरवार